गुरु पूर्णिमा का महत्व
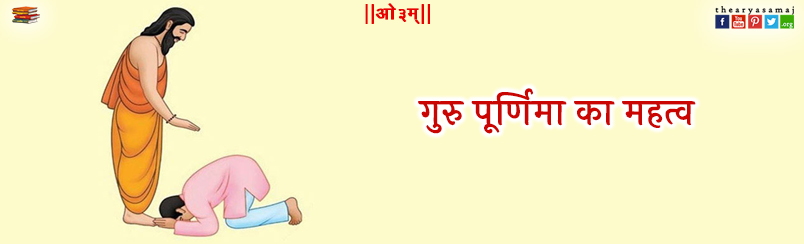

Author
Acharya AnoopdevDate
unknownCategory
लेखLanguage
HindiTotal Views
2084Total Comments
0Uploader
Vikas KumarUpload Date
16-Jul-2019Download PDF
-0 MBTop Articles in this Category
- फलित जयोतिष पाखंड मातर हैं
- राषटरवादी महरषि दयाननद सरसवती
- राम मंदिर भूमि पूजन में धर्मनिरपेक्षता कहाँ गई? एक लंबी सियासी और अदालती लड़ाई के बाद 5 अगस्त को पू...
- सनत गरू रविदास और आरय समाज
- बलातकार कैसे रकेंगे
Top Articles by this Author
गुरु का अर्थ
शास्त्रों में 'गु' का अर्थ बताया गया है – अंधकार या मूल अज्ञान और 'रु' का अर्थ किया गया है – उसका निरोधक।
गुरु को 'गुरु' इसलिए कहा जाता है कि वह अंधकार को हटाकर प्रकाश की ओर ले जाने वाले को 'गुरु' कहा जाता है।
इस जगत का सबसे बड़ा गुरु कौन है? इस प्रश्न का उत्तर हमें योग दर्शन में मिलता है –
"स एष पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्॥"
(योगदर्शन : 1.26)
वह परमेश्वर काल द्वारा नष्ट न होने के कारण पूर्व ऋषि-महर्षियों का भी गुरु है।
अर्थात – ईश्वर गुरुओं का भी गुरु है।
अब दूसरी शंका यह आती है कि क्या सबसे बड़े गुरु को केवल गुरु पूर्णिमा के दिन स्मरण करना चाहिए?
इसका स्पष्ट उत्तर है कि नहीं – ईश्वर को सदैव स्मरण रखना चाहिए और स्मरण रहते हुए ही सभी कर्म करने चाहिए।
अगर हर व्यक्ति सर्वव्यापी एवं निराकार ईश्वर को मानने लगे तो कोई भी व्यक्ति पापकर्म में लिप्त न होगा।
इसलिए धर्म शास्त्रों में ईश्वर को अपने हृदय में मानने एवं उनका उपासना करने का विधान है।
अब प्रश्न उठता है कि फिर गुरु कैसा हो, उसका व्यवहार कैसा हो, उसका आचरण कैसा हो, उसकी वाणी कैसी हो?
इसके लिए उपनिषदों में इस बारे में स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि –
"निवृत्तत्वन्यजनः प्रमादतः, स्वयं च निष्पापपथे प्रवर्त्तते।
गुणातितत्त्वं हितमिच्छुरंगिनां, शिवार्थिनां यः स गुरुर्निगद्यते॥"
भावार्थ –
जो दूसरों को प्रमाद करने से रोकते हैं, स्वयं निष्पाप रास्ते पर चलते हैं, जनहित और दीन-दुखियों के कल्याण की कामना का तत्त्व बोध कराते-कराते, तथा निस्वार्थ भाव से अपने शिष्य के जीवन को कल्याण पथ पर अग्रसर करते हैं – उन्हें गुरु कहा जाता है।
उन्नीसवीं शताब्दी का मध्यकाल – मथुरा में यमुनानदी के किनारे एक प्रज्ञाचक्षु गुरु विरजानन्द डंडी जी का आश्रम था।
जब अध्ययन पूरा होने के बाद जब स्वामी दयानन्द जी गुरु विरजानन्द जी को गुरु दक्षिणा के रूप में थोड़ी सी लौंग, जो गुरु जी को बहुत पसंद थी, लेकर गये, तो गुरु जी ने ऐसी दक्षिणा लेने से मना कर दिया। उन्होंने दयानन्द से कहा कि –
गुरु दक्षिणा के रूप में, मैं यह चाहता हूँ कि इस देश में जहाँ और धर्म के नाम पर पाखंड और अंधविश्वास का जाल फैला हुआ है।
भौली-भाली जनता अपनी अज्ञानता के अंधकार में सत्त्य के प्रकाश का इंतजार कर रही है, देश में धर्म के नाम पर फैले हुए पाखंड, अंधविश्वास और कुरूतियों को समाप्त करो।
गुरु जी के आदेश के अनुसार स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उत्थान में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।
हमारे जीवन में गुरु का महत्त्व माता-पिता के समान ही है,
और एक ही जीवन में हम एक अथवा अनेक गुरुओं से मिलते हैं और ज्ञान ग्रहण करते हैं।
जीवन को सद्मार्ग पर ले जाने वाला और एक सही दिशा देने में गुरु का ही सर्वोत्तम स्थान है।
इसलिए तो कहा गया है कि:
गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ि गढ़ि काढैं खोट।
अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहै चोट॥
अर्थ –
गुरु कुम्हार है और शिष्य मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है।
जिस तरह घड़े को सुंदर बनाने के लिए अंदर हाथ डालकर बाहर से थपकी दी जाती है,
ठीक उसी प्रकार शिष्य को कठोर अनुशासन में रखकर अंतर से प्रेम भावना रखते हुए
शिष्य की बुराइयों को दूर करके संसार में सम्मानीय बनाता है।




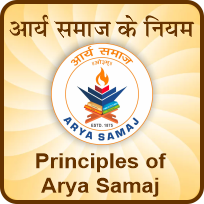







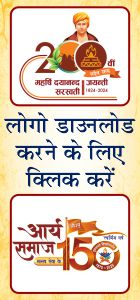
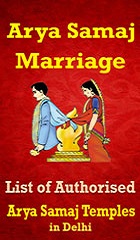
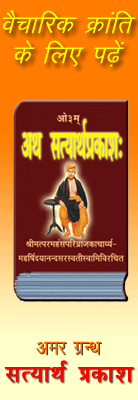



ALL COMMENTS (0)